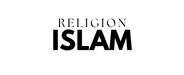हमारे प्रिय भाई,
पहला इंसान पहला पैगंबर भी है और
सभी पैगंबरों द्वारा लाई गई धर्म, अर्थात इस्लाम, भी एक ईश्वर में विश्वास करने वाला धर्म है।
प्राचीन काल में भी, जब विभिन्न जनजातियों ने अपने विश्वासों को बदल दिया और मूर्तिपूजा सहित विभिन्न धर्मों की ओर रुख किया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचीन काल में एक ईश्वर में विश्वास करने वाला धर्म मौजूद नहीं था। वास्तव में, वैज्ञानिक शोध प्राचीन काल से एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोगों की पुष्टि करते हैं। वैसे भी, इस विषय पर हमारा प्राथमिक स्रोत कुरान है।
ईश्वर में आस्था आदिम धर्मों और लगभग सभी अन्य विश्वास प्रणालियों में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे आदिम धर्मों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है, में किए गए शोधों के परिणामस्वरूप, प्रारंभिक विश्वासों के लिए फेटिशिज्म, टोटमिज़्म और एनिमिज़्म पर आधारित किए गए मानवशास्त्रीय व्याख्याओं में एक और व्याख्या जोड़ी गई है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित आदिम जनजातियों पर किए गए हाल के अध्ययनों, जो सबसे निचले सांस्कृतिक स्तर, सबसे प्राचीन चिंतन के तरीकों और मानव जीवन के सबसे असभ्य रूपों को दर्शाते हैं, ने यह साबित कर दिया है कि वे एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करते हैं।
प्राचीन मानवशास्त्रीय सिद्धांतों से व्याख्या करने योग्य न होने वाले एक विश्वास के अनुसार, एक सर्वोच्च ईश्वर जो मृत्यु से पहले से ही मौजूद था।
(जनता के पिता)
वह अभी भी आकाशा में विद्यमान है, लोगों और उनके व्यवहारों को देख रहा है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में एट्नातु लोगों के विश्वास के अनुसार, एक स्व-अस्तित्व वाला, आकाशा में रहने वाला, दयालु और शाश्वत ईश्वर मौजूद है। धर्मों के इतिहास के क्षेत्र में इस तरह के नए शोध इस बात को सिद्ध करते हैं कि आदिम विश्वासों में ईश्वर की एकता पर आधारित एक धारणा थी, और बहुदेववाद बाद में एक विचलन के रूप में सामने आया।
(देखें: God, ERE, VI, 243-247)
यह निष्कर्ष आकाशीय ग्रंथों के कथनों के साथ भी मेल खाता है।
हालांकि असीरियन-बाइबिल धर्म में बहुदेववादी विश्वास प्रणाली पाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से असीरियन लोगों के विश्वास के अनुसार, छोटे देवता सर्वोच्च देवता अशुर के सामने वास्तविक अस्तित्व नहीं हैं, बल्कि वे केवल उसके विभिन्न नामों में प्रकट होने वाले रूप हैं।
हालांकि यह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की अवधारणा नहीं है, लेकिन वास्तव में यह विषय इतना स्पष्ट और निश्चित नहीं है। मौजूदा जानकारी और दस्तावेजों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि बुद्ध ने स्वयं पारलौकिक दुनिया, रहस्योद्घाटन और परलोक जैसे धार्मिक विषयों पर ध्यान नहीं दिया, और प्राचीन भारतीय सांख्य दर्शन का अनुसरण करते हुए, ब्रह्मांड में ईश्वरीय हस्तक्षेप की अनुपस्थिति का आभास दिया। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को बुद्ध के जीवनकाल से सदियों बाद लिखा गया था। इसके अलावा, यह एक ज्ञात तथ्य है कि उनके इस रवैये से नास्तिकता का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है और न ही उनके अनुयायियों ने ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला। बाद के विकास में, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि बौद्ध धर्म ने ईश्वर की अवधारणा को अपनाया, यहाँ तक कि बुद्ध को स्वयं ईश्वर का दर्जा दिया गया।
चीन के धर्मों में पहले एक ईश्वर की मान्यता थी जो एकेश्वरवाद से मिलती-जुलती थी, लेकिन बाद में शंगटी नामक एक स्वर्गीय ईश्वर के साथ-साथ आकाश और पृथ्वी की आत्माओं की उपस्थिति को भी स्वीकार किया गया और इन आत्माओं को देवता के रूप में माना गया, जिससे बहुदेववादी दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव आया। हालाँकि, चीन में एक ईश्वर की मान्यता के क्षरण के खिलाफ अक्सर प्रतिक्रियाएँ भी हुई हैं।
यह निर्विवाद है कि प्राचीन मिस्र के धर्म में एक शक्तिशाली ईश्वर में विश्वास था, लेकिन यह कि क्या यह एक ईश्वर पर आधारित था, या एक प्रकार के बहुदेववाद (प्रत्येक जनजाति के लिए एक ईश्वर में विश्वास) पर आधारित था, यह शोधकर्ताओं के बीच बहस का विषय है। मिस्र के ग्रंथों में वर्णित ईश्वर,
“सब कुछ पैदा करने वाला, हमेशा से मौजूद, दुनिया का मालिक, जिसका ज्ञान असीम है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन दुआएँ सुनता है”
यह एक सर्वोच्च शक्ति है। हालाँकि, ये गुण कई देवताओं को भी समर्पित हैं। इन द्वितीय श्रेणी के देवताओं को एक ईश्वर के विभिन्न नामों और अभिव्यक्तियों के रूप में भी माना जा सकता है।
(देखें: ईआरई, खंड VI, पृष्ठ 275)
वास्तव में, कुरान में, हज़रत यूसुफ (अ.स.) ने मिस्र की जेल में बंद कैदियों को संबोधित करते हुए जो कहा था,
“तुम्हारे द्वारा अल्लाह के अलावा जिनों की इबादत की जाती है, वे केवल तुम्हारे और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा रखे गए नाममात्र के देवता हैं।”
(यूसुफ 12/40)
उसका यह कथन भी इसी अंतिम राय का समर्थन करता है।
ज़ैरोस्टर
ईसा पूर्व ईरानी लोगों ने आर्य जाति के रूप में हिंदुओं के साथ मूल रूप से समान विश्वास साझा किया। ज़रतुष्ट्र के अनुसार, ईश्वर…
(अहुरा मज़दा)
वह सर्वोच्च और अद्वितीय है, और उसका सार भौतिक नहीं है; वह दयालु और सर्वज्ञानी है, हर जगह मौजूद और देखरेख करने वाला है; वह परिवर्तन के अधीन नहीं है। हालाँकि, अहुर मज़्दा की शक्ति एक अर्थ में सीमित है। क्योंकि प्रकृति में उससे पूरी तरह से विपरीत एक आध्यात्मिक शक्ति भी है जो एक निश्चित अवधि में अहुर मज़्दा के कार्यों का विरोध कर सकती है और बुराई का कारण बन सकती है।
बाद में लिखे गए धार्मिक ग्रंथों में, अहुर मज़दा ने अपनी सर्वोच्चता तो बरकरार रखी, लेकिन अपनी पूर्ण एकता खो दी। पारंपरिक समझ में ईश्वर के गुणों के रूप में वर्णित विशेषताओं को व्यक्तिपरक बना दिया गया और उनकी पूजा की जाने लगी, यहाँ तक कि अग्नि को ईश्वर का पुत्र बताकर उसकी भी पूजा की जाने लगी। इसके अलावा, ज़रोथेस्ट्री धर्म से पहले के देवताओं से मिलते-जुलते प्रकृति देवताओं को याज़ता कहा गया और उनकी भी अहुर मज़दा और उसके मुख्य स्वर्गदूतों के साथ पूजा की जाने लगी। यह ज़रोथेस्ट्री धर्म की मूलतः एकेश्वरवादी अवधारणा से एक विचलन है।
प्राचीन तुर्कों की राष्ट्रीय परंपरा में, प्रतीकात्मक अर्थों वाले जानवरों, जैसे भेड़िया और गरुड़, के प्रति दिखाए गए ध्यान से प्रेरित होकर, कुछ शोधकर्ताओं ने उनके धर्म में टोटमवाद के तत्वों की खोज की है, हालाँकि यह ज्ञात है कि तुर्कों का सामाजिक, कानूनी और आर्थिक जीवन टोटमवाद के निर्धारित ढाँचों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, स्टेपी तुर्क मान्यताओं और शमांवाद के बीच संबंध स्थापित करने का मामला एक स्थापित लेकिन अधूरा दृष्टिकोण है। क्योंकि शमांवाद को धर्म होने के बजाय जादू की प्रकृति वाली एक समाधि तकनीक के रूप में वर्णित किया गया है। चिकित्सा, मृत आत्माओं से संपर्क करना और उनके नुकसान को दूर करना, और जिन्न और परियों के साथ संबंध स्थापित करना जैसे उद्देश्यों के लिए इस तरह की तकनीकों को, कई आदिम धर्मों की तरह, स्टेपी तुर्क मान्यताओं में भी शामिल माना जाता है। हालांकि, फिर भी प्राचीन तुर्कों में शमांवाद उनके धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त व्यापक कार्य नहीं करता प्रतीत होता है। यही स्थिति उन व्याख्याओं के लिए भी है जो प्राचीन तुर्कों को, जो अपने पूर्वजों की यादों को पवित्र मानते थे, एक प्रकार के पूर्वज पूजा से संबंधित मानते हैं। वास्तव में, मृत पूर्वजों को अर्द्ध-देवता मानना, उन्हें मानव बलि देना, या मृत पूर्वज के पास उसकी पत्नी और उसके दल के किसी सदस्य को दफनाना जैसे पूर्वज पूजा के विशिष्ट विश्वास और प्रथाएँ प्राचीन तुर्कों में नहीं पाई गई हैं।
स्थलवासी तुर्क समुदाय का मूल धर्म आकाश के ईश्वर में विश्वास करना और उसकी पूजा करना है। इस विश्वास प्रणाली में
“टेन्ग्री” (भगवान)
उसे एक सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान प्राणी माना गया, उसकी महिमा को दर्शाने के लिए उसे “आकाशीय” कहा गया और आमतौर पर उसे आकाश देव कहा जाता था। वह ईश्वर जो मनुष्यों के भाग्य का निर्धारण करता है, जीवन में सीधे हस्तक्षेप करता है, आदेश देता है और जो उसके आदेश का पालन नहीं करता उसे दंडित करता है, जीवन का सिद्धांत है और मृत्यु भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। ईश्वर कानून है, सत्य है; मनुष्य नश्वर हैं, वह शाश्वत और अनंत है। इन सभी गुणों के साथ-साथ ईश्वर एक है। प्राचीन तुर्क धर्म से संबंधित सभी डेटा शोधकर्ताओं को इस विश्वास प्रणाली के एक ईश्वर सिद्धांत पर आधारित होने के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वास्तव में, तुर्कों द्वारा इस्लाम धर्म को कम समय में और बड़े पैमाने पर अपनाने में, अन्य कारकों के साथ-साथ, उनके पुराने विश्वासों और इस्लाम में ईश्वर की एकता के सिद्धांत के बीच एक समानता या निकटता देखने का भी प्रभाव रहा है।
इस्लाम से पहले अरबों के मूर्तिपूजा करने के बारे में जाना जाता है। कुरान में इस विषय पर बार-बार चर्चा की गई है, और कुछ आयतों में मूर्तियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है।
(देखें, उदाहरण के लिए, अल-नज़्म 53/19-20; अल-अ’राफ 7/180; राजी, तफ़सीर, IV, 477)
हालांकि, यह भी समझा जाता है कि उनका मानना था कि विभिन्न जनजातियों से संबंधित सैकड़ों मूर्तियों के ऊपर एक सर्वोच्च ईश्वर है। कुरान, उनके शब्दों में,
“अल्लाह”, “अज़ीज़”
और
“अलीम”
उन्होंने बताया कि वे उस सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसे वे इस नाम से पुकारते हैं, और जो उन्हें और पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सूर्य और चंद्रमा को एक निश्चित व्यवस्था में बांधा है, और वर्षा करके पृथ्वी को जीवों के पोषण के लिए अनुकूल बनाया है।
(देखें, उदाहरण के लिए, अल-अंकेबूत, 29/61, 63; अल-ज़ुह्रुफ, 43/9),
साथ ही, उन्होंने ईश्वर की कसम खाई थी।
(अल-अनआम 6/109; अल-नहल 16/38)
, उन्होंने अपने जीवन के कठिन और खतरनाक समय में उसी में शरण ली।
(अनाऊ 6/40-41; युनुस, 10/22)
और उन्होंने उसे काबा का भगवान माना।
(कुरैश, 106/3)
यह बयान करता है। कुरान यह भी बताता है कि जाहिलिया काल के अरबों का इस सर्वोच्च ईश्वर (अल्लाह) में विश्वास के साथ-साथ मूर्तियों की पूजा करना इस विश्वास पर आधारित था कि मूर्तियाँ उन्हें अल्लाह के करीब ले जाएंगी और अल्लाह के पास उनके लिए सिफारिश करेंगी (देखें यूनुस 10/18; ज़ुमर, 39/3)। कुछ अन्य आयतें, जाहिलिया काल के अरबों को…
“सर्वोच्च ईश्वर”
यह अल्लाह में विश्वास के अन्य संकेतों को भी छूता है, जिसका अर्थ है ईश्वर में विश्वास।
(देखें: जवाद अली, अल-मुफस्सल, खंड VI, पृष्ठ 104-105)
कुछ लेखकों का कहना है कि जाहिलिया काल के अरबों में पाई जाने वाली सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा यहूदियों और ईसाइयों के प्रभाव से बनी थी, या कम से कम इस प्रभाव ने इस अवधारणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
(इज़ुत्सु, पृष्ठ 99-105)
यद्यपि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, जो मूलतः एकेश्वरवाद पर आधारित हैं, के इस तरह के प्रभाव सैद्धांतिक रूप से संभव प्रतीत होते हैं, लेकिन इस्लाम से पहले के अरबों में विदेशी प्रभावों के प्रति खुले धर्म की खोज की भावना का अभाव और यहूदियों और ईसाइयों दोनों के साथ उनके नकारात्मक या उदासीन संबंध, इस दृष्टिकोण की सत्यता को बहुत कम संभावना प्रदान करते हैं। जैसा कि ज्ञात है, अरबों के अपने देश में ईसाई बहुत कम थे। यस्रिब (मदीना) के आसपास बसने वाले यहूदी कबीले भी उस क्षेत्र के अरबों द्वारा इस हद तक गर्मजोशी से नहीं माने गए थे कि वे उनके प्रभाव में आ जाएं।
इसके अतिरिक्त, अरबों की मूर्तिपूजा और सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा में न तो यहूदी आदमखोरवाद और न ही ईसाई त्रिएकवाद के निशान देखे जा सकते हैं। इसलिए, इस्लाम से पहले के अरबों के धार्मिक जीवन में देखी गई सर्वोच्च ईश्वर की आस्था को हज़रत इब्राहिम (अ.स.) से बचे हुए हनीफ धर्म से जोड़ना अधिक उचित होगा। वास्तव में, हज़रत पैगंबर (स.अ.व.) और कई अन्य अरब कबीलों की वंशावली इब्राहिम (अ.स.) के पुत्र इस्माइल (अ.स.) तक पहुँचती है। विभिन्न आयतों के कथन से यह समझा जा सकता है कि हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) ने शाश्वत मुक्ति को लक्ष्य बनाकर एक सार्वभौमिक आह्वान के साथ प्रकट हुए, और इस आह्वान को हनीफ के रूप में संक्षिप्त रूप से कहलाने वाले विश्वास पर स्थापित किया, जिसे उनके द्वारा संबोधित समुदाय ने स्वीकार कर लिया था। इसके विपरीत, बहुदेववादियों और विशेष रूप से यहूदियों और ईसाइयों ने इब्राहिम (अ.स.) के धर्म (मिल्लत) के प्रति अपनी वफ़ादारी का दावा किया; कुरान-ए-करीम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इब्राहिम (अ.स.) यहूदी, ईसाई या बहुदेववादी नहीं थे, बल्कि वे अल्लाह को एक मानने वाले मुसलमान (हनीफ-मुस्लिम) थे।
(आल-ए-इमरान 3/67),
उन्होंने बताया कि मार्गदर्शन और मुक्ति केवल इब्राहिम (अ.स.) के धर्म का पालन करके ही प्राप्त की जा सकती है, और उन्होंने पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) और यहूदियों, ईसाइयों और बहुदेववादियों सभी को इस धर्म का पालन करने का आदेश दिया।
(देखें: एमएफ अब्दुलबाकी, मु’जम, “हनीफ”, “हुनेफा” मदें)
नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी कहा कि उन्होंने जो धर्म प्रचार किया, वह यहूदी धर्म या ईसाई धर्म नहीं, बल्कि एक सहिष्णु एकेश्वरवादी धर्म (अल-हनीफिय्या अल-समहा) था (मुस्नद, V, 266; VI, 116, 233) और उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य धर्म में ये विशेषताएँ होनी चाहिएं।
(बुखारी, “ईमान”, 29; तिरमिज़ी, “मनकीब”, 32, 64; मुसनद, 1, 236)
सभी आकाशीय धर्मों के मूल्यांकन के अनुसार, पैगंबरों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हज़रत इब्राहिम (अ.स.) के धर्म के प्रति वफ़ादार रहने वाला एकमात्र धर्म, अंतिम पैगंबर द्वारा प्रचारित इस्लाम है। हज़रत मुहम्मद (स.अ.व.) का पैगंबर बनने से पहले का धार्मिक जीवन और उनके पहले अनुयायियों के दिलों की गहराई में स्थित विश्वास भी इसी धर्म के करीब था। उन्होंने अपने सार्वभौमिक आह्वान को इसी विश्वास के आधार पर स्थापित किया और इसीलिए वे सफल हुए।
(डीआईए. अल्लाह एमडी. विभिन्न धर्मों में ईश्वर की आस्था)
मानव इतिहास के शोधों में यह देखा गया है कि एकेश्वरवाद मूल विश्वास था, और बहुदेववाद और मूर्तिपूजा जैसे विश्वास बाद में लोगों में फैले। विपरीत विचार कभी भी सच्चाई को नहीं दर्शाते हैं।
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर
टिप्पणियाँ
नमस्ते41
मेरा भी यही मानना है कि यहाँ पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का तात्पर्य सच्चे मुसलमान से है, अर्थात् वे मुसलमान जो सुन्नत-ए-सानीया को अपने जीवन में लागू करते हैं और अपने जीवन को सीधे रास्ते पर बिताते हैं और बड़े पापों से दूर रहते हैं।