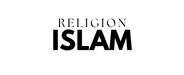1. दारुलइस्लाम में रहने वाले गैर-मुस्लिम किस किताब/धर्म के अनुसार न्याय प्राप्त करते हैं? इसका प्रमाण क्या है?
2. गैर-किताबी लोगों का न्याय किस आधार पर किया जाएगा?
3. काफ़िरों के आपसी मामलों में किस प्रकार के न्याय का प्रयोग किया जाता है? (क्या उन्हें इस्लाम के अनुसार या उनके अपने धार्मिक नियमों के अनुसार न्याय पाने की स्वतंत्रता है? इस बारे में क्या फैसला है?)
4. गैर-मुस्लिमों के साथ मुसलमानों के बीच विवादों में, किस प्रकार के नियमों से उनका न्याय किया जाता है? (क्या उन्हें इस्लाम के अनुसार या उनके अपने धार्मिक नियमों के अनुसार न्याय पाने की स्वतंत्रता है? इस बारे में क्या फैसला है?)
हमारे प्रिय भाई,
शासन, प्रभुत्व, सत्ता
इसे किसी राज्य की आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या निगरानी के बिना शासन और कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है।
राज्य की आंतरिक संप्रभुता, अर्थात् देश और देश में रहने वालों पर राज्य का अधिकार
आंतरिक प्रभुत्व
, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी हस्तक्षेप और निगरानी के बिना कार्य करने की भी
विदेशी प्रभुत्व
या इसे स्वतंत्रता कहा जाता है।
राज्य की आंतरिक सर्वोच्चता की एक आवश्यकता के रूप में
न्यायिक अधिकार और कर्तव्य उस राज्य के हैं जो इस्लामी समुदाय की ओर से राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतिनिधित्व और अभ्यास करता है।
से संबंधित है।
(निस़ा 4/105; माईदा 5/48; साद 38/26)
इस्लामी देश में स्थित
मुस्लिम या गैर-मुस्लिम, नागरिक या विदेशी, सभी लोग राज्य की न्याय प्रणाली और कानूनों के अधीन हैं।
obedient है।
हालांकि, इस्लाम द्वारा गैर-मुस्लिमों को दी गई विश्वास की स्वतंत्रता की एक आवश्यकता के रूप में
परिवार, व्यक्ति, उत्तराधिकार और ऋणों के कानून जैसे धार्मिक विश्वासों से निकटता से जुड़े विषयों पर
जिन्हें न्यायिक और कानूनी रूप से अधिकार दिया गया है, हनाफी फ़कीरों के शब्दों में, इस मामले में
“उन्हें अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना”
(सरास़ी, अल-मबसू़त, XI, 102; कासानी, II, 311)
इस सिद्धांत को अपनाया गया है।
इस्लाम द्वारा स्थापित यह कानूनी बहुलवाद, धार्मिक-सांस्कृतिक बहुलवाद की रक्षा करके गैर-मुस्लिमों को सदियों से इस्लामी समाज में अपनी उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति देता रहा है।
गैर-मुस्लिम, उनमें से
जिस तरह से उन्हें अपने कानूनी विवादों को अपने न्यायालयों में ले जाने का अधिकार है, उसी तरह से इस्लामी न्यायालयों में भी।
वे भी मुकदमा दायर कर सकते हैं।
गैर-मुस्लिम समुदायों के भीतर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को, बहु-कानूनी व्यवस्था के दायरे में, स्वयं द्वारा ही हल किया जाना चाहिए।
उनके द्वारा नियुक्त या नामित न्यायाधीशों द्वारा, उनके अपने धार्मिक नियमों के अनुसार
समाधान हो गया है। राज्य ने एक कानूनी सिद्धांत के रूप में जिम्मी लोगों को अपने धर्मगुरुओं को चुनने और प्रशिक्षित करने के अधिकार को मान्यता दी, उनके द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि को वैध प्रतिनिधि माना और इसलिए उनके द्वारा दिए गए फैसलों को भी वैध फैसलों की श्रेणी में रखा।
हालांकि, उन्होंने जिम्मी लोगों को मुस्लिम न्यायाधीशों के पास जाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा। ऐसे मामलों में, मुस्लिम न्यायाधीशों को विशेष रूप से भूमि विवादों जैसे मामलों को देखते हुए पाया गया है।
[देखें: वेकी’, मुहम्मद बिन हलफ बिन हय्यान, (306/918), अह्बारु’ल-कुदात, I-III, बेरूत, अनुवाद, III, 88; II, 281]
पक्षों में से एक मुस्लिम है।
यदि ऐसा हो तो, मामले को सुनने के लिए एकमात्र सक्षम न्यायालय
यह एक इस्लामी न्यायालय है।
गैर-मुस्लिमों और राज्य के बीच या गैर-मुस्लिमों और मुसलमानों के बीच होने वाले विवादों में (धार्मिक नियम के रूप में) मुस्लिम न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में, न्यायाधीश एक सिद्धांत के रूप में,
मुस्लिम-गैर-मुस्लिम के बीच भेदभाव नहीं करता, सभी पक्षों को कानून के समक्ष समान मानता है।
वे स्वीकार करेंगे।
वास्तव में, इस्लाम के प्रारंभिक काल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ मुस्लिम न्यायाधीशों ने कई मामलों में गैर-मुस्लिमों के पक्ष में फैसला दिया। इस संदर्भ में, राज्य के प्रमुख (खलीफा)
वह कहानी जिसमें एक यहूदी ने हज़रत अली की शिकायत क़ाज़ी शूरेह से की थी।
यहाँ हम एक उदाहरण दे सकते हैं। वादी यहूदी और प्रतिवादी राज्य प्रमुख, कूफ़ा के क़ाज़ी शूरेह द्वारा प्रशासित क़ानूनी सभा में आते हैं। खलीफ़ा क़ाज़ी के पास बैठना चाहता है; न्यायाधीश उसे चेतावनी देता है और उसे वादी के पास बिठा देता है। यहाँ तक कि एक कहानी के अनुसार, इस मामले में उसने खलीफ़ा के खिलाफ फैसला सुनाया।
इसी तरह, एक ही जज के ज़िमी पड़ोसी ने जब किसी मुसलमान के घर को खरीदने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उस मुसलमान ने अपना घर किसी और को बेच दिया, तो जज ने ज़िमी को घर बेचने के कारण बिक्री को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने ज़िमी के शिफा अधिकार का सम्मान नहीं किया था।
(देखें वेकी’, II , 389)
दोनों पक्ष गैर-मुस्लिम हों
और यह कि क्या इस्लामी न्यायालय में अपील करने पर न्यायालय को इस मामले को देखने की स्वतंत्रता है या नहीं, यह विद्वानों के बीच बहस का विषय है।
हनाफी मत के अनुसार,
पक्षकारों के ज़िमी या मुस्तैमन होने की परवाह किए बिना, दायर किए गए मामले की सुनवाई और निपटान किया जाना चाहिए; न्यायालय के पास चयन का अधिकार नहीं है।
मालिकी और हनबली संप्रदायों के अनुसार
तो न्यायालय मामले की सुनवाई करने में स्वतंत्र है; पक्षकार ज़िमी या मुस्तैमन हैं
(पासपोर्ट वाले गैर-मुस्लिम विदेशी)
धर्म चाहे समान हो या अलग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमद इब्न हंबल से यह भी कहा गया है कि जिम्मी लोगों के मामलों को भी सुना जाना चाहिए।
शाफीई मत के अनुसार,
यदि दोनों पक्ष मुस्त’मंन हैं, तो न्यायाधीश को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है; लेकिन यदि एक या दोनों पक्ष ज़िमी हैं, तो प्रबल मत यह है कि मामले की सुनवाई की जानी चाहिए।
जिन लोगों ने तर्क दिया कि न्यायालय को इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है,
“यदि वे तुम्हारे पास आएँ, तो या तो उनमें फैसला करो, या उनसे मुँह मोड़ लो। यदि तुम उनसे मुँह मोड़ लोगे, तो वे तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और यदि तुम फैसला करो, तो उनमें न्यायपूर्वक फैसला करो। क्योंकि अल्लाह न्याय करने वालों को प्यार करता है।”
(अल-माइदा, 5/42)
जबकि कुछ लोग इस आयत को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो अन्य लोग…
“उनमें अल्लाह के द्वारा उतारे गए क़ानून के अनुसार फ़ैसला करो और उनकी इच्छाओं का अनुसरण मत करो।”
(अल-माइदा 5/49)
वे उस आयत को आधार बनाते हैं जिसमें यह कहा गया है कि एक आयत ने दूसरी आयत को निरस्त कर दिया है।
इस समूह के कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यहाँ निरसन (नस्ह) का कोई मामला नहीं है, बल्कि पहली आयत मुस्त’मन (मुस्लिम शरणार्थियों) से संबंधित है और दूसरी आयत ज़िमी (मुस्लिम शासन के अधीन रहने वाले गैर-मुस्लिम) से संबंधित है।
कानूनी जानकार कहते हैं कि न्यायालय को मुस्तैमन के मामलों को देखने में स्वतंत्रता है, और वे यह भी कहते हैं कि वे एमानत समझौते के माध्यम से इस्लामी नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, और न ही इस्लामी राज्य उनके बीच अन्याय को रोकने की गारंटी देता है।
अन्य कानूनी विद्वान कहते हैं कि मुस्त’मन, ज़िमी की तरह, इस्लामी राज्य की सुरक्षा के अधीन हैं और राज्य को उन पर होने वाले अन्याय को रोकना चाहिए।
कोर्ट में केस की सुनवाई के लिए
क्या दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है?
फिर से यह चर्चा का विषय बन गया है।
हनाफी मत के अनुसार, चाहे वह जिम्मी हो या मुस्तैमन, केवल एक पक्ष का मुकदमा दायर करना पर्याप्त है। मालिकी मत के अनुसार, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है।
शाफ़ी और हनबली संप्रदाय ज़िमी लोगों के मामले में केवल एक पक्ष की सहमति को आवश्यक मानते हैं, जबकि मुस्त’मन लोगों के मामले में दोनों पक्षों की सहमति को आवश्यक मानते हैं।
इस मामले में विवाद आम तौर पर इस बात पर आधारित होते हैं कि क्या किसी एक पक्ष के आवेदन पर दूसरे पक्ष को उसकी अपनी आस्था के विपरीत एक निर्णय मानने के लिए बाध्य किया जा सकता है या नहीं।
यदि इस्लामी न्यायालय गैर-मुस्लिमों के मामले की सुनवाई करता है, तो उनके अपने कानून के बजाय इस्लामी कानून लागू किया जाएगा।
इस विषय पर विभिन्न आयतों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने वाले इस्लामी विद्वान
(उदाहरण के लिए, देखें अल-माइदा, 5/42, 44, 48)
वे एकमत हैं।
सामान्य नियम के अनुसार, गैर-मुस्लिमों पर लागू होने वाला कानून का नियम मुसलमानों पर लागू होने वाले नियम के समान ही है। हालाँकि, वे अपने विश्वास के अनुसार जो वैध मानते हैं…
सूअर और शराब
जैसे कि संपत्ति से संबंधित लेनदेन और कुछ अन्य मामलों में, जो वे स्वयं वैध मानते हैं, वे अलग-अलग नियमों के अधीन हैं। इन विषयों पर कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी अलग-अलग राय हैं।
(देखें अहमद ओज़ेल, इस्लामी कानून में देश की अवधारणा, इस्तांबुल 1991, पृष्ठ 355-364)
गैर-मुस्लिमों को कानूनी मामलों के लिए दी जाने वाली न्यायिक और कानूनी प्रतिनिधित्व की अनुमति
यह आपराधिक मामलों पर लागू नहीं होता है।
इस लिहाज से, जब वे किसी इस्लामी देश में अपराध माना जाने वाला कोई काम करते हैं, तो सामान्य तौर पर उन्हें भी
इस्लामी दंड संहिता के प्रावधान
लागू किया जाता है।
लेकिन उन्हें दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के कारण इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद हैं। उदाहरण के लिए
यदि शराब पीने पर सज़ा नहीं दी जाती है
यदि वे सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दंडात्मक सजा दी जाएगी।
इसके अलावा, कुछ अपराधों के घटित होने के लिए आवश्यक शर्तों का गैर-मुस्लिमों में न होना, जो कि विभिन्न संप्रदायों के अनुसार भिन्नता रखते हैं, के कारण उन्हें उन अपराधों के लिए निर्धारित सजा नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए, अबू यूसुफ को छोड़कर हनाफी विद्वानों के अनुसार, पत्थर मार कर मारने की सजा के लिए आवश्यक शर्तें…
इहसान
चूँकि इस शर्त के लिए मुसलमान होना आवश्यक है, इसलिए यदि जिम्मी लोग व्यभिचार करते हैं, तो उन्हें पत्थर मार कर नहीं, बल्कि कोड़े मारकर दंडित किया जाता है।
ज़िम्मी के विपरीत, मुस्तैमन पर दंड संहिता के लागू होने के संबंध में अलग-अलग मत व्यक्त किए गए हैं। अबू यूसुफ ने कहा कि ज़िम्मी की तरह मुस्तैमन पर भी दंड संहिता के सभी प्रावधान लागू होंगे, जबकि अन्य धर्मशास्त्रियों ने, जिनमें अलग-अलग मत हैं, अपराधों को अल्लाह (समाज) के अधिकार या व्यक्ति के अधिकार के विरुद्ध होने के आधार पर वर्गीकृत किया है और सामान्य तौर पर कहा है कि समाज के अधिकार के प्रबल होने पर दंड मुस्तैमन पर लागू नहीं होंगे।
इस मामले में मतभेद इस बात पर केंद्रित है कि एक मुस्तैमिन, जो अस्थायी रूप से एक इस्लामी देश में रह रहा है, किन नियमों का पालन करने के लिए उत्तरदायी है।
(देखें: Özel, पृष्ठ 369-372; TDV İslam Ansiklopedisi, Gayri Müslim, Zimmi md.)
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर