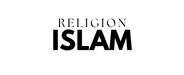उदाहरण के लिए, जब किसी की उंगली पर खून का एक बूँद होता था, तो वह हनाफी की तरह व्यवहार करता था या शाफी की तरह? संप्रदायों के बनने का कारण क्या है और संप्रदायों के बनने से लोगों को क्या लाभ हुए हैं?
हमारे प्रिय भाई,
इस्लाम में धार्मिक नियमों के दो स्रोत हैं:
पुस्तक
और
लिंगछेदन।
इन दोनों के बाद आवेदन किया जाएगा।
तुलना
और
इक्मा
मूल रूप से, यह भी इन्हीं दो स्रोतों पर निर्भर है। इन चारों पर एक साथ
“चार सिद्धांत, चार धार्मिक प्रमाण”
उन्हें नाम दिया जाता है। सभी धार्मिक निर्णय इन चार प्रमाणों से निकाले जाते हैं, इसलिए वे इन पर आधारित होते हैं। ये चार प्रमाण क्रम से इस प्रकार हैं:
1. पुस्तक:
पुस्तक से तात्पर्य कुरान-ए-करीम से है। इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, हमारा पवित्र ग्रंथ, जिस प्रकार अल्लाह द्वारा अवतरित किया गया था, उसी प्रकार संरक्षित है, इसमें एक अक्षर भी नहीं बदला है। क्योंकि, इसके संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर ने ली है और इसे सुरक्षित रखा है। इसलिए, धार्मिक मामले में सबसे पहले कुरान-ए-करीम से ही परामर्श किया जाना चाहिए।
2. छंटनी:
सुन्नत से तात्पर्य है पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के पवित्र वचन, कार्य और वे स्थितियाँ जिनमें उन्होंने कुछ देखकर भी मना नहीं किया और मौन धारण किया। पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की इन स्थितियों को, जिन्हें सुन्नत कहा जाता है, हदीस भी कहा जाता है।
सहाबी
कुरान में निहित धार्मिक नियमों के विवरण से संबंधित हजारों हदीसों को याद करके और संरक्षित करके, उन्होंने उन लोगों को प्रेरित किया जो उनके बाद आए और
“ताबीउद्दीन”
उन्होंने इसे दूसरी पीढ़ी को बताया, जिसे कहा जाता है। सबसे पहले हिजरी 101 में उमर बिन अब्दुल अजीज के प्रयासों से धार्मिक नियमों के विवरण से संबंधित लगभग चार हजार हदीस-ए-शरीफ एकत्र किए गए थे। कुरान के बाद, सुन्नत धार्मिक नियमों को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. तुलना:
किसी एक मामले में स्थापित किसी निर्णय के समान निर्णय को, दूसरे मामले में इत्तिहाद के अंत में प्रकट करना है। दूसरे शब्दों में,
पुस्तक, मुंडन
या
इक्मा
किसी मुद्दे पर जो फैसला तय हो चुका है, उसे उसी कारण और उसी तर्क पर आधारित किसी दूसरे समान मुद्दे पर लागू करना है।
तुलना,
लेकिन यह काम केवल एक विद्वान कर सकता है जो मुज्तहिद के स्तर का हो।
4. इंजमा:
इज्मा
एक ही सदी में रहने वाले इस्लामी विद्वानों का किसी मुद्दे पर धार्मिक निर्णय के बारे में सहमत होना।
इसके अनुसार, कुरान और सुन्नत में, जिस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, उस मामले में विद्वानों द्वारा दिए गए फैसलों में सहमति होने पर, वह फैसला
“इज्मा-ए-उम्मत”
इसका मतलब है कि वह बात निश्चित हो गई है। जिस बात पर इमामा (सर्वसम्मति) हो गई है, वह अब एक मजबूत बात बन गई है। इस बात का उल्लेख निम्नलिखित हदीसों में भी किया गया है:
“मेरी उम्मत कभी भी कुपथ पर सहमत नहीं होगी।”
1
“जो चीज़ मुसलमानों को अच्छी लगती है, वह अल्लाह के पास भी अच्छी होती है।”
2
इत्तिहाद-मुज्तहिद:
आराधना और लेनदेन से संबंधित किसी नियम को धार्मिक प्रमाण से निकालने के लिए प्रयास करना
इक्तहाद
कहते हैं। और जो विद्वान इन नियमों को उनके प्रमाणों से निकालता है, उसे
मजहबी विद्वान
उसे नाम दिया जाता है।
मुज्तहद
उसे कुरान, सुन्नत और इस्लामी कानून से संबंधित सभी मामलों में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के समय से ही, जब इस्लाम के विद्वानों को किसी धार्मिक निर्णय की आवश्यकता होती थी और उन्हें कुरान और सुन्नत में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता था, तो उन्होंने अपने इत्तिहाद (न्यायिक निर्णय) का सहारा लिया। हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने साथियों को इस मामले में अनुमति दी थी। वास्तव में, जब हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने अपने साथियों में से विद्वान और फकीह मुआज़ बिन जबेल (रा) को यमन का गवर्नर नियुक्त किया, तो उन्होंने उनसे पूछा:
“जब तुम वहाँ पहुँचोगे, तो तुम किस आधार पर न्याय करोगे? जब तुमसे कोई सवाल किया जाए या कोई वादी तुम्हारे पास आए, तो तुम उस समस्या का समाधान कैसे करोगे?”
मुआज़:
“अल्लाह की किताब कुरान के साथ।”
रसूलुल्लाह:
“अगर तुम्हें किताब में नहीं मिलता?”
मुआज़:
“रसूलुल्लाह की सुन्नत के अनुसार।”
रसूलुल्लाह:
“अगर तुम्हें वहाँ भी न मिले?”
मुआज़:
“अगर मुझे उसमें भी नहीं मिलता है, तो मैं अपने विवेक से फैसला करूँगा।”
इस पर रसूल-ए-अकरम (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कहा:
“भगवान की कृपा से, पैगंबरों के दूत (मुआज़) को पैगंबरों की इच्छानुसार सफलता मिली।”
उन्होंने मुआज़ के इन शब्दों पर अपनी खुशी व्यक्त की।3
जब पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) जीवित थे, तब सहाबा के बीच कोई मतभेद नहीं था। अगर धर्म के सिद्धांतों और शाखाओं में सहाबा में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आती थी, तो वे पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से पूछते थे और वे उसे समझाते थे।
जब हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) इस दुनिया से चले गए, तब कुरान और सुन्नत सहाबीयों के याद में थे। लेकिन सहाबीयों में से जो कुरान और सुन्नत को अच्छी तरह से जानते थे, उनके नियमों और अर्थों को अच्छी तरह से समझते थे, वही फतवा देते थे। इन्हें सहाबीयों के विद्वान और फकीह कहा जाता है।
उमर, अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, आयशा, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू मूसा अल-अशारी
इनमें से सबसे प्रसिद्ध थे।
चार खलीफा के शासनकाल में और बाद के समय में, मुसलमान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इन लोगों के पास जाते थे, और वे कुरान और सुन्नत के अनुसार निर्णय देते थे; यदि उन्हें इन दोनों में समाधान नहीं मिलता था, तो वे “कयास” (तुलनात्मक तर्क) के माध्यम से समस्या का समाधान करते थे। इस प्रकार, सहाबा के समय में कई मामलों में “इज्मा” (सर्वसम्मति) स्थापित हो गई; इस्लामी कानून, फिकह का गठन हुआ।
इस बीच, इन सहाबीयों ने कुछ शहरों में बसकर अपने ज्ञान और विद्वता से इस्लाम की सेवा की। उदाहरण के लिए, हज़रत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद ने कूफ़ा में, अनस बिन मालिक और अबू मूसा अल-अशारी ने बसरा में, और अब्दुल्ला बिन उमर और ज़ैद बिन साबित ने मदीना में सैकड़ों छात्रों को शिक्षित किया। इन सहाबीयों द्वारा शिक्षित इन छात्रों को…
“ताबीउद्दीन”
कहा जाता है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की छोड़ी हुई ज्ञान की विरासत इस पीढ़ी को मिल गई। इनमें से कई विद्वान ऐसे थे जो इत्तिहाद करने के स्तर तक पहुँच गए थे। उदाहरण के लिए, इब्राहिम अन-नहाई, हसन अल-बसरी, तावूस बिन कासन उनमें से कुछ हैं।
ताबीउद्दीन
उन्होंने सहाबीयों द्वारा वर्णित हदीसों और उनके इत्तिहाद को एकत्रित किया और एक साथ रखा। इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ आयत, हदीस और सहाबीयों के इत्तिहाद मौजूद नहीं थे, उन्होंने स्वयं भी इत्तिहाद किया। उन्होंने अपने आसपास के छात्रों को शिक्षित करने की कोशिश की। उन्होंने इस्लामी कानून की नींव रखने, नई समस्याओं का विस्तार से अध्ययन करने और उनके फैसलों को स्पष्ट करने में अपने छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस पीढ़ी को भी…
“तबे-ए-ताबीन”
उसे यह नाम दिया गया है।
इमाम-ए-आज़म, इमाम-ए-मालिक, इमाम-ए-शाफ़ी, अहमद बिन हनबल, सुफ़यान-ए-सवरि, सुफ़यान बिन उययना
ये इस पीढ़ी के प्रसिद्ध लोगों में से हैं। इनमें से इमाम-ए-आज़म ने कुछ सहाबीयों को देखा था, लेकिन अपनी विद्वता के आधार पर वे तबे-ए-ताबीईन में शामिल हैं।
यही वह समय है जब फ़िक़ही मज़हबों का गठन हुआ। तबे-ए-ताबीईन के इमामों ने सहाबा और ताबीईन के इत्तिहाद को एकत्रित किया। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने भी कई मामलों में इत्तिहाद किया। मुसलमानों के सामने आने वाले हज़ारों मामलों पर उन्होंने चिंतन किया और कुछ सिद्धांत स्थापित किए। ये लोग विभिन्न शहरों में रहते थे और अपने विद्वतापूर्ण कार्य अपने निवास स्थान पर करते थे।
दूसरी ओर
प्रत्येक की फतवा पद्धति अलग-अलग थी। कुछ केवल कुरान और सुन्नत को आधार मानते थे, कुछ इसके साथ-साथ क़ियास को भी स्वीकार करते थे; कुछ कुरान, सुन्नत और सहाबा के इमा के प्रकाश में अपने राय से फतवा देते थे। कुछ ने अपने क्षेत्र के रीति-रिवाजों को भी ध्यान में रखा। इस तरह के इत्तिहाद और फतवों ने मुसलमानों के धार्मिक जीवन को काफी आसान कर दिया था।
इल्म-ए-इत्तिहाद के इन विद्वानों के ये इत्तिहाद इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि द्वितीय श्रेणी के गौण मामलों पर आधारित थे। समय के साथ, एक ही मुद्दे पर कई अलग-अलग इत्तिहाद और व्याख्याएँ सामने आईं। मुसलमानों ने अपने क्षेत्र में रहने वाले इल्म-ए-इत्तिहाद के विद्वान के इत्तिहाद को स्वीकार किया और उसके अनुसार अपनी इबादत और लेनदेन की ज़िन्दगी जीई।
यह प्राथमिकता और पक्षपात, समय के साथ अपनी जगह खो देता है
“अपनाया गया रास्ता”
जिसका अर्थ है
“मत”
उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। वह युग कई इस्लामी शास्त्रों, विशेष रूप से हदीस और तफ़सीर की शिक्षा के लिए एक उपजाऊ भूमि थी। मुजतहिद स्तर के कई विद्वान मौजूद थे। चूँकि हर मुजतहिद की राय और फ़तवा को स्वीकार करने और मानने वाले लोग थे, इसलिए अंत में हर इमाम को एक संप्रदाय का प्रतिनिधि माना गया। इस स्थिति ने अंततः सैकड़ों संप्रदायों के अस्तित्व में आने का कारण बना।
समय के साथ, जिन विद्वानों ने बाद में इमामों का दर्जा प्राप्त किया, उनमें से अधिकांश ने उन इमामों के मजहब को अपनाया जिन्हें उन्होंने अपने से अधिक विद्वान माना या जिन इमामों के साथ वे किसी मुद्दे पर एकमत थे। वैसे भी, किसी भी मजहब के संस्थापक विद्वान ने…
“हमने एक संप्रदाय स्थापित किया है, हमारा अनुसरण करो, हमारे संप्रदाय को स्वीकार करो, और उस संप्रदाय को मेरे नाम से कहो।”
उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई आह्वान या उपदेश नहीं दिया। वे केवल अपने सभाओं में आने वाले लोगों को धार्मिक विज्ञान सिखाते थे और उनके सामने आने वाले मुद्दों के समाधान खोजने की कोशिश करते थे। जब उनसे किसी मुद्दे के धार्मिक निर्णय के बारे में पूछा जाता था, तो वे उसे स्पष्ट करते थे। इन इमामों से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, और विद्वान और जनता जो उनके शब्दों और व्याख्याओं को स्वीकार करते थे, उनके अनुयायी बन जाते थे। इस तरह उनके शब्द और व्याख्याएँ एक संप्रदाय बन गईं।
क्योंकि ये सम्मानित व्यक्ति इत्तिहाद करते समय अपने स्वार्थी और संकीर्ण विचारों से पूरी तरह दूर रहते थे। उनमें विद्वतापूर्ण अहंकार और कट्टरता नहीं थी। वे सत्य, सही और सुंदर को जहाँ भी पाते, उसे स्वीकार कर लेते थे।
मुज्तहिदों द्वारा किए गए इक्तहादों के एक मजहब बनने और फैलने में उनके शिष्यों का बहुत योगदान रहा। इसलिए कुछ इमामों के शिष्यों ने अपने गुरुओं के इक्तहादों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करके एक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि कई अन्य इस मामले में उतनी सफलता नहीं दिखा सके।
शुरुआत में अस्तित्व में आए कई संप्रदाय, अनुयायियों और छात्रों की कमी के कारण अंततः जीवित नहीं रह सके और केवल किताबों के पन्नों में ही सीमित रह गए।
आज, अहले सुन्नत के संप्रदायों में से चार जीवित हैं:
इमाम अबू हनीफा और हनफी मत, इमाम मालिक और मालिकी मत, इमाम शाफी और शाफी मत, इमाम अहमद बिन हनबल और हनबली मत।
स्रोत:
1. इब्न माजा, फ़ितन: 8.
2. मुसनद, I/379.
3. तिरमिज़ी, अहकाम: 3; अबू दाऊद, अक़दीया: 11; इब्न माजा, मनासिक: 38.
(देखें: मेहमेद पाक्सु, इबादत हमारी ज़िंदगी)
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर