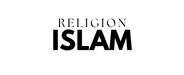– क्या आप इस बात की व्याख्या कर सकते हैं कि सलमान फ़ारसी ने फ़ातिहा सूरे का फ़ारसी में अनुवाद क्यों किया और इमाम आज़म ने फ़ातिहा सूरे के फ़ारसी अनुवाद को नमाज़ में पढ़ने की अनुमति क्यों दी?
हमारे प्रिय भाई,
लेकिन सरहसी द्वारा वर्णित हज़रत सलमान की घटना, पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जीवनकाल में और उनकी अनुमति से नहीं हो सकती। क्योंकि कहा जाता है कि अज़म के लोगों का इस्लाम में प्रवेश पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के निधन के बाद हुआ था।
इसके अलावा, इमाम-ए-आजम का यह फतवा कि नमाज़ में फ़ातिहा सूरे का फ़ारसी अनुवाद पढ़ा जा सकता है, एक विशेष स्थिति से संबंधित है:
यह उन लोगों के लिए है जो इस्लाम के केंद्र से दूर रहते हैं।
एक कथा के अनुसार, यह फ़ारसी भाषा में अनुवाद के लिए ही उपयुक्त है, जिसे स्वर्ग की भाषा माना जाता है।
फतीहा के लिए विशेष रूप से छूट दी गई है। ताकि जो लोग फतीहा नहीं जानते, वे नमाज़ छोड़ें नहीं।
ईमान की ताकत से पैदा हुई भावना से फातिहा के पवित्र अर्थों को समझना चाहने वालों के लिए यह जायज माना गया है। जबकि, ईमान की कमजोरी और कुरान की भाषा अरबी के प्रति घृणा से पैदा हुई भावना से फातिहा का अनुवाद करना और अरबी मूल को छोड़ देना, धर्म को छोड़ना है!
यह भी बताया गया है कि इमाम आजम ने बाद में इस फतवे से अपना मत बदल दिया था।
नमाज़ में अनिवार्य क़िरात किस भाषा में होनी चाहिए, यह विषय ज़्यादातर फ़िक़ह के सिद्धांतों की किताबों में चर्चा किया गया है। कुरान-ए-करीम के केवल अर्थ ही नहीं, बल्कि उसके शब्दों का भी वही दिव्य, पवित्र और अद्वितीय (मु’ज़िज़) स्वरूप है, इस पर सहमति है। नमाज़ में कुरान का पाठ करना अनिवार्य है, इस पर भी कोई मतभेद नहीं है। कुरान-ए-करीम में यह भी बताया गया है कि कुरान अरबी भाषा में है। इन दोनों आदेशों को एक साथ रखने पर जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि “नमाज़ में कुरान का पाठ उसी भाषा में करना अनिवार्य है जिसमें वह अवतरित हुआ था”। हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने भी यही फरमाया है। चूँकि अनुवादित पाठ मूल पाठ के समान नहीं होता, इसलिए जो व्यक्ति फ़ातिहा का अनुवाद पढ़ता है, वह फ़ातिहा का पाठ नहीं करता।
इन तर्कों पर आधारित सभी विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जो व्यक्ति अरबी में नमाज़ पढ़ सकता है, उसके लिए नमाज़ में किसी अन्य भाषा में पाठ करना जायज़ और मान्य नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा ने अपने एक ऐसे फतवे में कहा था, जिसे बाद में उन्होंने वापस ले लिया था। अबू हनीफ़ा के इस फतवे का आधार क्या था, इसका प्रमाण क्या था, यह उन्होंने स्वयं स्पष्ट नहीं किया। उनके नाम पर व्याख्या करने वाले कुछ धर्मशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण कमज़ोर पाए गए हैं। हनाफ़ि मत अबू हनीफ़ा का नहीं, बल्कि अबू यूसुफ़ और मुहम्मद जैसे अन्य हनाफ़ि विद्वानों सहित बहुमत के फतवे को अपनाता है, और इस मत में इसी के अनुसार फतवा दिया जाता है; इस नियम में अकेले नमाज़ पढ़ने वाले और इमाम के रूप में नमाज़ पढ़ने वाले तथा जत्थे के साथ नमाज़ पढ़ने वाले के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।
नमाज़ में क़िरात के मसले का फ़िक़ह में यही फ़ैसला है। कुछ धर्मशास्त्री, धार्मिक और शास्त्रीय कारणों की बजाय राजनीतिक, वैचारिक और व्यावहारिक कारणों और उद्देश्यों से नमाज़ में क़िरात के तुर्की भाषा में होने का समर्थन करते हुए, फ़िक़ह में क़िरात के विषय को समझाते समय जानबूझकर कुछ भ्रांतियाँ और छल-कपट करते हैं। इनमें से जो हमारे ध्यान में आए हैं, उनका -सही बात बताते हुए- उल्लेख इस प्रकार है:
केवल नूह बिन मरयम ने ही अबू हनीफा के इत्तिहाद से रजू (वापसी) की बात नहीं कही है। उदाहरण के लिए, अबू यूसुफ के छात्रों में से अली बिन अल-जाद ने भी इसे बयान किया है। केवल नूह बिन मरयम का उल्लेख करना और यह साबित करने की कोशिश करना कि वह एक विश्वसनीय वृत्तांतकर्ता नहीं है, एक छल है।
सरहसी ने अपनी कृति “मेबसूत्” में अबू हनीफ़ा के इत्तिहाद का उल्लेख करने के बाद यह भी लिखा है कि इमाम ने इसे मकरूह माना था। इसे न बताना, छिपाना ईमानदारी के विपरीत है। इसी कृति में सलमान फ़ारसी के फ़ातिहा का फ़ारसी में अनुवाद करने और अज़म के लोगों के अरबी भाषा में पारंगत होने तक अपनी नमाज़ में इस अनुवाद को पढ़ने का उल्लेख किया गया है। इस कथन का यह भाग जनता से छिपाना विद्वता के आचार के अनुकूल नहीं है। अरबी पढ़ने में असमर्थ लोगों के लिए, जब तक वे अरबी में पारंगत न हो जाएँ, दूसरी भाषा में पढ़ने की अनुमति कई इमामों द्वारा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। सरहसी ने फ़िक़ह उस्सूली के क्षेत्र में अपनी कृति “उस्सूली” में भी इस विषय पर चर्चा की है और संक्षेप में निम्नलिखित मूल्यांकन किया है: कुरान-ए-करीम का शब्द और अर्थ दोनों अद्वितीय हैं, उनका कोई समान नहीं बनाया जा सकता। इस मामले में हनाफी इमामों का एकमत है। नमाज़ में पढ़ने के संबंध में; दो छात्रों के इमाम के अनुसार, दोनों तत्वों (अर्थात शब्द – जो अरबी है – और अर्थ) की क़िराअत में उपस्थिति आवश्यक है। अनुवाद से पढ़ने पर केवल अर्थ (एक तत्व) मौजूद हो सकता है, जो अरबी पढ़ने में सक्षम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके गुरुओं के अनुसार, दोनों तत्व पवित्र और अद्वितीय हैं, लेकिन जब केवल एक (केवल अर्थ) मौजूद होता है तो यह नमाज़ के लिए पर्याप्त होता है; लेकिन चूँकि यह पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की सुन्नत और सदियों के अभ्यास के विपरीत है, इसलिए अनुवाद से पढ़ना मकरूह है।
सेराहसी ने ‘अल-मेबसूत’ में अबू हनीफा के ‘रूजू’ (पुनर्विचार) का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ‘अल-महित’ और ‘अल-जामी अस-सागिर’ की व्याख्या में ‘रूजू’ की उस कहानी को शामिल किया है।
सरहसी द्वारा वर्णित हज़रत सलमान की घटना, हमारे पैगंबर (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के जीवनकाल में और उनकी अनुमति से घटित नहीं हो सकती। क्योंकि कहा जाता है कि ईरानियों के इस्लाम में प्रवेश पैगंबर के निधन के बाद हुआ था।
अल-अंसारी ने अपनी उस्सूली किताब “मुसलैमूस-सुबूत” पर जो व्याख्या लिखी है, उसमें हसन अल-बसरी के मित्र हबीब अल-अजमी नामक एक इस्लामी विद्वान का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने अरबी भाषा में महारत हासिल नहीं की थी और अरबी नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अनिवार्य कुरान की पाठ फ़ारसी में की थी। इस कथन को उद्धृत करने वाले कुछ धर्मशास्त्रियों द्वारा इसका एक भाग छोड़ देना एक छल है।
कुछ धर्मशास्त्री, फिक़ह की किताबों में जो वे ढूंढ रहे थे, वह न मिलने पर इतिहास और यात्रा वृत्तांत की किताबों का सहारा लेते हैं और उनसे जानकारी लेकर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। जबकि सही इबादत के मामले में, सहाबा के दौर के बाद के अमल सबूत नहीं हो सकते। इसके अलावा, इस अमल की संभावना हमेशा मौजूद रहती है।
प्रसिद्ध तफ़सीरकार ज़माख़शरी ने अबू हनीफ़ा के इस मत पर महत्वपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है: उनके अनुसार, इसका जायज़ होना इस शर्त पर निर्भर करता है कि अरबी भाषा के शब्दों में निहित अर्थ को पूरी तरह से दूसरी भाषा में अनुवादित किया गया हो। चूँकि वे फ़ारसी भाषा नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इस संभावना के आधार पर फ़तवा दिया था। हम जानते हैं कि यह संभव नहीं है; इसलिए उनका कहना, उनके कहने के बराबर है, इसी अर्थ में है।
जिन लोगों ने फقه की किताबों और सही संप्रदाय के फ़तवों को तो दूर, सही हदीसों को भी तब तक नहीं माना जब तक कि उन्हें अपने काम में न आएं, और जिन्होंने गैर-धार्मिक कारणों और उद्देश्यों से निर्णय और फ़ैसला किया, उन लोगों का इस बात को साबित करने के लिए फقه की ओर लौटना, संप्रदाय में छोड़े गए इत्तिहाद का सहारा लेना, और उन ऐतिहासिक वृत्तांतों और प्रथाओं को सबूत के तौर पर पेश करना जिनकी सच्चाई और विवरणों की जांच करना संभव नहीं है, एक सबक सिखाने वाला व्यवहार का उदाहरण है।
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें:
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर