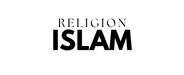हमारे प्रिय भाई,
राष्ट्रीय मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से ऊपर रखने वाली, राष्ट्र के प्रति निष्ठा को सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण मानने वाली, और राष्ट्रीय हितों को व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण मानने वाली विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का सामान्य नाम।
राष्ट्रवाद
यह अपने राष्ट्र से प्रेम करने और उसे ऊंचा उठाने के उद्देश्य से लेकर, अपनी जाति को अन्य सभी जातियों से श्रेष्ठ मानकर उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा तक, विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है। इसलिए, यह किसी विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम या सिद्धांत से अधिक, ऐसे कार्यक्रमों और सिद्धांतों को मानने वाले सभी राजनीतिक दृष्टिकोणों को व्यक्त करता है।
हमारे देश में
लगभग हर क्षेत्र में अवधारणाओं में व्याप्त भ्रम, खुद को
“राष्ट्रवाद”
यह अवधारणा में भी स्पष्ट है। इसलिए, सबसे पहले अवधारणा और नाम के बीच की विसंगति और विरोधाभास को निर्धारित करना आवश्यक है।
राष्ट्र
शब्द, कुरानिक अर्थ के अनुसार
“धर्म”
और
“शरिया”
शब्दों का अर्थ समान है। शब्द का प्रयोग केवल एक निश्चित समुदाय को दर्शाने के लिए रूपक रूप से किया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी, स्वाभाविक रूप से, यह किसी जनजाति, जाति या राष्ट्र को नहीं, बल्कि धर्म और शरीयत में विश्वास करने वाले और उससे जुड़े सभी लोगों को दर्शाता है, जैसा कि इसके वास्तविक अर्थ द्वारा निर्धारित किया गया है: इसके अनुसार, शब्द का व्युत्पन्न, राष्ट्र, धर्म और शरीयत को दर्शाता है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। राष्ट्रवाद, उसी धर्म और शरीयत के प्रति समर्पण का नाम है। जबकि आज के सामान्य उपयोग में, शब्द को उसके मूल अर्थ को अनदेखा करके इस्तेमाल किया जाता है,
“राष्ट्र”
इसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है और इससे बहुत भ्रम पैदा हो रहा है। क्योंकि
“राष्ट्र”
यह किसी विशेष विश्वास, धर्म और धार्मिक कानून को नहीं, बल्कि एक वंश से आने वाले लोगों को संदर्भित करता है।
इसलिए, राष्ट्र से जुड़ाव पर आधारित समझ और दृष्टिकोणों को राष्ट्रवाद शब्द से नहीं, बल्कि अर्थ के अनुरूप रूप से राष्ट्रवाद या
राष्ट्रवाद
शब्दों से नामित किया जा सकता है।
इस्लाम ने रक्त संबंध, रिश्तेदारी और संबंधों के महत्व को अस्वीकार नहीं किया। इनको स्वीकार करते हुए, इसने इन संबंधों को मजबूत करने और रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रावधान किया। इसलिए कुरान में मुसलमानों को रिश्तेदारी के बंधन तोड़ने से मना किया गया है:
“… अल्लाह से और (रिश्तों को) काटने से (रिश्तों को तोड़ने से) बचा करो।”
(एन-निसा, 4/1)।
हालांकि, इस्लाम इस बात की अनुमति नहीं देता कि रिश्तेदारी के बंधन, और बाद में राष्ट्रीय बंधन, समाज को निर्धारित करने और संबंधों को विनियमित करने के मुख्य सिद्धांत बन जाएं। इस्लाम द्वारा परिकल्पित समाज रक्त संबंध, वंश या हितों के एकीकरण जैसे भौतिक आधारों पर नहीं बनाया जा सकता;
मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से और उनकी इच्छा के विरुद्ध मौजूद गुण, इस्लामी समाज के निर्णायक सिद्धांत नहीं हो सकते।
इस्लाम के अनुसार, समाज के निर्माण और व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों के नियमन में एकमात्र निर्णायक सिद्धांत वह विश्वास है जिसे लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से चुनकर अपनाते हैं।
विश्वास का बंधन इस्लामी समाज की नींव है।
सभी व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियाँ और विशेषताएँ केवल इस साझा विश्वास, साझा बंधन में ही अर्थ प्राप्त करती हैं। विश्वास द्वारा एकजुट न किए गए लोगों के बीच रक्त संबंध, वंश की एकता जैसे सभी बंधन अपना अर्थ और वैधता खो देते हैं। कुरान इस तथ्य को हज़रत नूह (अ) की कहानी के माध्यम से स्पष्ट और निश्चित रूप से प्रस्तुत करता है। समान विश्वास को साझा न करने वाले लोगों को न केवल एक ही समाज का, बल्कि एक ही परिवार का सदस्य भी नहीं माना जा सकता:
“नूह ने पुकारा, ‘हे मेरे पालनहार! मेरा बेटा मेरे परिवार का है, और तुम्हारा वचन सत्य है, और तुम न्यायियों के न्यायी हो।’ (परमेश्वर) ने कहा, ‘हे नूह! वह तुम्हारे परिवार का नहीं है, वह तो कुकर्मी है। जो बात तुम नहीं जानते, वह मुझसे मत मांगो। मैं तुम्हें अज्ञानी लोगों में से न होने की सलाह देता हूँ।”
(हूद, 11/45-46).
जब तक विश्वास में एकता नहीं होती, तब तक रक्त संबंध, जो सबसे मजबूत होता है, परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को भी तोड़ देता है, पारस्परिक अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं:
“तुम अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखने वाले समुदाय को, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए नहीं पाओगे, भले ही वे उनके पिता, पुत्र, भाई या रिश्तेदार ही क्यों न हों।”
(संघर्ष, 58/22)।
हे लोगो! यदि वे ईमान के मुकाबले कुफ्र को पसंद करते हैं, तो अपने बाप और भाइयों को वली मत बनाओ। जो तुम में से कोई उनको वली बनाएगा, वही ज़ालिम है।
(अत-ताउबा, 9/23)।
इन व्यापक नियमों के भीतर, हर मुसलमान का लक्ष्य केवल तुर्क-इस्लामी एकता नहीं, बल्कि सभी मुसलमानों की एकता होनी चाहिए। सभी मुसलमानों की एकता में मुस्लिम तुर्क भी शामिल होते हैं।
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर