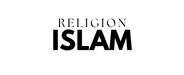हमारे प्रिय भाई,
न्यायालय में अर्जी दाखिल करने वाले किसी एक पक्ष द्वारा दायर किया गया मुकदमा, और न्यायाधीश द्वारा तलाक का कारण मानकर उन्हें अलग करने के लिए दिया गया निर्णय, समकालीन फिक़ह साहित्य में…
“भेदभाव”
के रूप में व्यक्त किया गया है। शास्त्रीय फقه स्रोतों में यह न्यायालय का निर्णय
“समाप्ति”
को भी इसी तरह से माना जाता है।
न्यायालय द्वारा दिए गए “तलाक” के निर्णय के कुछ मुख्य कारण हैं। ये हैं: पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण (भोजन, वस्त्र और आवास) न देना, उसे वास्तव में छोड़ देना, किसी एक साथी में यौन संबंध में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति का होना और पति-पत्नी के बीच अनबन होना। हम यहाँ अन्य विवरणों में जाने के बिना, आज सबसे अधिक तलाक का कारण बताए जाने वाले अनबन के कारण, किसी एक साथी द्वारा न्यायालय में की गई याचिका का मूल्यांकन करेंगे।
हाफ़िज़, शाफ़ी और हंबली के अनुसार,
चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों न हो, असहमति
“भेदभाव”
ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता, और न ही न्यायालय ऐसा कोई निर्णय ले सकता है। उनके अनुसार, पति द्वारा पत्नी को पीटना, उसे प्रताड़ित करना, उसे अपमानजनक शब्दों से ठेस पहुँचाना, बिना किसी उचित कारण के उससे रूठकर उसे छोड़ देना, उससे मुँह मोड़ लेना, जैसे कारण जो वैवाहिक असहमति का कारण बनते हैं, को न्यायालय के निर्णय से दूर करना, विवादों का समाधान करना, और पति को दंडात्मक उपायों से – यूँ कहें तो – सुधरना और अत्याचार से बाज आना संभव है। इन उपायों से परिवार को बचाना आवश्यक है। (अल-फिक्हुल-इस्लामी, V/527).
मालिकी के अनुसार,
अमेल-असंगति तलाक का एक कारण है और यदि न्यायालय शिकायतकर्ता के दावों को सही पाता है, तो वह पति-पत्नी के बीच “विच्छेद” का आदेश देगा।
इन विद्वानों के अनुसार, “परिवार को नरक में बदलने वाली अनबन” को तलाक का कारण मानकर औरतों को “अलग” करना,
“इस्लाम में किसी को नुकसान पहुँचाना और नुकसान के बदले में नुकसान पहुँचाना नहीं होता।”
यह सिद्धांत के अनुरूप भी है।
न्यायालय के आदेश से पति-पत्नी को अलग करने वाला यह “तफ्रीक” निर्णय, रिज्ई नहीं, बल्कि बाइन तलाक माना जाता है (देखें: आगे)।
कुछ स्रोतों के अनुसार, हनबली विद्वान भी मालिकी विद्वानों की तरह ही सोचते हैं (देखें: इल्मीहाल-इस्लाम और समाज, TDVY, II/236)। कुछ शाफी विद्वान भी विशेष रूप से इस मत के हैं कि पति द्वारा पत्नी को आवश्यक निर्वाह प्रदान न करने की स्थिति में यह तलाक का एक कारण है। लेकिन अधिकांश हनफी विद्वानों की तरह ही सोचते हैं (इब्न अबीदिन; III/590)।
आपके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है:
गैर-मुस्लिम देश में, गैर-मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय – यदि वह इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप हो – तो मुसलमानों के लिए भी बाध्यकारी है।
निस्संदेह, किसी मुसलमान के लिए सबसे उचित यही है कि वह अपनी ज़रूरत के किसी मामले में अपने जैसे किसी मुसलमान न्यायाधीश/न्यायालय से संपर्क करे। लेकिन गैर-मुस्लिम देशों में रहने वाले लोगों के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में, ज़रूरी हालात में इन लोगों के लिए उस देश के न्यायालयों से संपर्क करना और (जब तक कि वह इस्लाम के स्पष्ट रूप से विपरीत न हो) दिए गए फैसलों के अनुसार कार्य करना जायज़ है। क्योंकि किसी देश में रहना उस देश के (इस्लाम के विपरीत न होने वाले) रीति-रिवाज़ों और नियमों को मौन/अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का ही अर्थ है। और यह,
“जो चीज़ परम्परागत रूप से जानी जाती है, वह उसी तरह है जैसे कि जो चीज़ शर्त के रूप में तय की गई हो।”
यह फقهي नियम के अनुरूप भी है, जो इस प्रकार है:
वास्तव में, इज़्ज़ बिन अब्दुलसलामा, इब्न तैमिया और शातिबी जैसे प्रसिद्ध फ़िक़ह विद्वानों के अनुसार, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए, फ़ित्ने-फ़साद को दूर करने के लिए, और सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में अराजकता को रोकने के लिए, आवश्यक परिस्थितियों में, गैर-मुस्लिम न्यायाधीशों/न्यायालयों के निर्णय का पालन करना जायज़ है। (यह तथ्य कि मानवीय कानून के कई नियम इस्लामी नियमों के विपरीत नहीं हैं, को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे “इस्लाम के विपरीत नहीं…” जैसे वाक्यांशों को इसी संदर्भ में समझा जाना चाहिए।) (देखें: क़रा रतुल्-मेज्लीसी’ल-उरब्बी लील-इफ़्ता वल्-बुहूस, 3/16/1426-25/4/2005)।
सलाम और दुआ के साथ…
इस्लाम धर्म के बारे में प्रश्नोत्तर